नयार की लहरों का लेखा-जोखा ‘मल्यो की डार’ – अनिल कार्की
गीता गैरोला की संस्मरण पुस्तक की समीक्षा
स्मृतियाँ हमारे जेहन में कभी स्थिर नहीं रहती वे तरल होती हैं। वे गतिशील
जीवन से ससन्दर्भ जुड़ने लगती हैं। वे हमारे अवचेतन में करवट बदलती रहती हैं। उम्र
के साथ उनके अर्थ व सन्दर्भ संश्लिष्ट ही नहीं, बहुआयामी भी होते जाते हैं। स्मृति
हमारी पक्षधरता के साथ समकालीन सन्दर्भों से जुड़ जाती है। स्मृति ठीक उन मिथकों
की तरह इस्तेमाल होने लगती हैं, जिन्होंने अतीत से वर्तमान
की यात्रा करते हुए, अपने सैद्धान्तिक स्वरूपों व दार्शनिक
अर्थों को खुद ही तोडा़ और खुद ही गढ़ा भी। इतिहास व आस्था के दायरों में बने रहने
के बावजूद भी मुझे लगता हैं कि स्मृति एक अलग तरह की मिथक
हैं, जो घटित होने के बाद भी स्वरूप और दृष्टी के लिये तरसती
रहती हैं। आगत समयों में वे अपने घटित होने के लम्बे अन्तराल में जब दृष्टि पाती
हैं और समय का दबाव जब उसे देखने के लिये राजनैतिक पक्षधरता प्रदान करता है तो वह ’मल्यो की डार’ जैसे एक अलग दस्तावेज और अलग विधा का
रास्ता अख़्तियार कर लेती है, जो अपार संवेदना से भरे लोक के
साथ ही शहरों के अजनबीपन को पूरी तरह
व्यक्त करता है। अपनी खास वैचारिकी से और वर्तमान सन्दर्भ के साथ ही जीवन
के गहरे जाकर चीजें छूने और उन्हे समझने की छटपटाहट का सग्रंह है ’मल्यो की डार’। जिसका शिल्प और लय का प्रस्थान
बिन्दु, अपार संवेदनाओं वाले मनुष्य और तकनीकी समय में मशीन
बनते मनुष्य के साथ ही वर्तमान वैश्वीकरण के अन्तरद्वंद्व से उपजा है।
खैर यह तो निशचित ही हैं कि परिधि की छिटकी अस्मिताओं, वंचित, समूहों के लिये स्मृति बहुत काम का औजार हो
सकती है। स्मृतियाँ स्त्रियों के साथ दलित तबकों का इतिहास लिखा सकती हैं, पर इसके लिये बहुत सचेत होना होगा। गीता गैरोला बहुत सचेत होकर पूरी किताब
में उन बिन्दुओें को छूती हैं, जिनमें स्त्रियां हैं, आम
किसान, मजदूर हैं और बाजार व अभिजातीय तबकों द्वारा लील लिया
गया एक सरलमना मनुष्य है। यह किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ जीवन में विचार
है, विचार में जीवन नहीं, न अतिस्त्रीवादी आग्रह और न ही मशीनी सिद्धान्त के प्रति जबरन मोहग्रस्तता। हाँ,
यह जरूर है कि यह किताब एक खास किस्म की स्त्रियों के अन्तरमन को
पूरा उकेर के सामने रख देती हैं। इधर कुमाऊँ की तरफ ब्राह्मण स्त्री का साहित्य
में आया जो सबसे प्राभवी मेरे जेहन में उभर के आता है, वह है गुरुवर शैलेश
मटियानी की कहानी सुहागिन का, लेकिन मैं चकित हूँ कि सुहागिन
के बाद अगर हमें कहीं फिर दुबारा से कोई इतना सघन प्रभावी चित्र और स्वानुभूत सत्य
मिलता हैं तो वह है गीता गैरोला का संस्मरण ’घने कोहरे के बीच’,
बहुत गज्जब का संस्मरण है यह, जो धीरे धीरे
वर्ग का जातीय चरित्र खोल के सामने रख देता है। ’माई फूफू’
जैसी गुमनाम औरत के बहाने हम पहाड़ में स्त्री शोषण का कच्चा चिठ्ठा
पढ़ पाते हैं।
“बच्चों के मोह मे फंसी माई कब जीजा के मोह जाल में उलझ गयी, पता ही नहीं
चला। जीजा को बच्चों की आया के साथ ही अपना दिल बहलाने के लिये एक खूबसूरत खिलौना
मिल गया इस रिश्ते को न तो जीजा ने कोई नाम दिया न माई के माईके वालों ने ही कोशिश
की। जाने कितने जाड़े कितनी बरसातें निकल गई। नयार में पता नहीं कितने बरसातों का
पानी बह गया।”
गीता ने पन्द्रह अगस्त के बहाने जहाँ आज के उथले राष्ट्रवाद को शुरूआती
ईमानदार राष्ट्रवाद के बरक्स देखने की कोशिश हैं, वहीं वे
अपने बेटे के बहाने अपने बचपन में पहूँच के कर्जु भैजी जैसा चरित्र पकड़ लाती हैं,
जो पन्द्रह अगस्त को स्कूल के सूट सिलता हैं और पूरे गाँव के लिये
दलित हैं। आजादी के इस मोड़ में पीछे छूट गये लाखों लाख लोगों को प्रतिनिधित्व
करते कर्जु के बहाने गीता ने पहाड़ी सामन्ती समाज की जो झाँकी प्रस्तुत की वह बहुत
अधिक विश्वसनीय ही नही प्रामाणिक भी है।
“मेरे बचपन में कपड़े सिलने का
काम औजी किया करते थे गाँव के पूरे मवासे उनकी वृति में बँटे रहते थे….उनकी
जजमानी बँधी रहती थी इसके लिये उन्हें मजदूरी देने का रिवाज नहीं था।”
’देवताओं का खेल’ अपनी स्मृति-कोष को दुरस्त करता और
मौखिक परम्परा को ग्रहण करने का शुरूआती खेल प्रतीत होता है। संम्भव है जो पहाड़
में पैदा हुआ हो उसने जरूर देवताओं का खेल खेला ही होगा, उनकी
नकल की ही होगी। ’मल्यो की डार’ संस्मरण
भी परम्परा ग्रहण की शुरूआती तालीम का संस्मरण है, जब पुरखे
खेल-खेल में हमें परम्परा का हस्तातंरण कर देते थे और हमें उसका अन्दाजा तक न होता
था। मल्यो की डार पढ़ते हुए मैं स्वयं भी अपने बचपन के आँगन लौट आया। ’कुणाबुड’ के बहाने एक प्रयोगधर्मा दादा का चरित्र
उभर के सामने आया है, जो पहाड़ों में फैले अन्धविश्वास को नकारता है। इन सब
संस्मरणों में लोक के इतने सघन बिम्ब है कि पूरा परिवेश चरितार्थ होने लगता है। ’मेरे मास्टर’ जी कई कई ढंग से पहाड़ के जातिवाद व
स्त्री विरोधी मानसिकता का पर्दा उठाता संस्मरण है, जिसमें
गुमनाम संघर्षशील प्रयोगधर्मा शिक्षक अन्थवाल मास्टर को गीता ने एक बार पुनः जीवित
कर दिया है। एक शिक्षक के सामाजिक दायित्व बोध के मानकों पर खरा यह मास्टर किस तरह
दलित बच्चों के द्वारा लाया पानी पाने के बाद आलोचनाओं में घिर जाता है, किस तरह वह लड़कियों को भाषण और गीत नृत्य सिखाने पर लाँछित होता है इसका
कच्चा चिट्ठा है यह संस्मरण।
मैं शुरू मैं ही कह आया हूँ कि मैं स्मृतियों राजनैतिक चीज मानते हुए, उन्हें किसी खास समय के विरुद्ध
खड़ा करना चाहता हूँ। पहाड़ों में हिन्दू-मुस्लिम गंगाजमुनी परम्परा के बहुत मोहक उदाहरण मिलाते हैं पर जब से राम ने भाजपा
ज्वाइन की तब से लगातार वैमनस्य बढ़ता सा गया है। गीता गैरोला के ’नजीब दादा’ इसी गंगाजमुनी परम्परा के वाहक है। वैसा
चूड़ी बेचने वाला मामूली सा अपार संवेदनाओं भरा पात्र पुनः केन्द्र में दिखाई देता
है। जिसकी पहनाई चूड़ियाँ गीता को आज भी याद हैं। ’मल्यो की
डार’ एक अजब संस्मरण है, स्मृतियों का
अजायबघर है। जिसके हर पन्ने में पहाड़ की विहंगम झाँकिया दिखाई देती हैं। चख्कू, चौमास, बिजी जा, स्याही
की टिक्की, आ ना मासी धंग, एक रामलीला
ऐसी भी, सामूहिकता का रिवाज, नखलिस्तान,
गाँव के तरफ, सभी संस्मरण विषयवस्तु के साथ ही
विधागत दृष्टि से भी अद्भुत है। गीता ने जगह जगह पर लोकगीतों का भी प्रयोग
खूबसरती से किया है।
इधर पहाड़ में लम्बे समय से इतने प्रभावी और नपे तुले संस्मरण मेरे देखने
में नहीं आये है, जो एक अलग तरह की बहस की माँग करते हैं।
हमारा लोक केवल महान ही नहीं है, उसमें भी सामन्ती और स्त्री
विरोधी व्यवस्थायें हैं, जातिवाद गहरे तक जड़ें जमाये बैठा
है। तमाम किस्म के सवालों से जूझता यह संग्रह ’मल्यो की डार‘
इस समय की एक जरूरी किताब हैं, जिसे नयार नदी
के लहरों का लेखा- जोखा कहा जा सकता है, जो सभ्यता के मुहाने
से वर्तमान तक पहुँची हैं। इस किताब को पढ़ते हुए मैने महसूस किया कि कम से कम हमारी
नई पीढ़ी को इस किताब तक जाना ही चहिए और इस बहाने आज के पहाड़ पर बात होनी चाहिए।
प्रकाशक – समय साक्ष्य,
15 फालतु लाईन देहरादून।
पृष्ठ संख्या-158, मूल्य 200 रुपयें मात्र
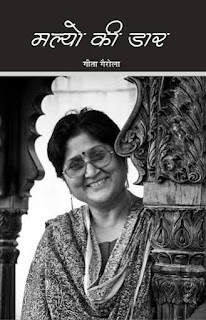
बेहद सटीक समीक्षा…., बधाई अनिल और गीता दोनों को…!
बहुत बहुत आभार तुम दोनों का शिरीष अनिल
गीता जी की पुस्तक मल्यो की डार की अच्छी समीक्षा की है अनिल कार्की जी ने| पुस्तक मैंने पढ़ी है| इस पुस्तक में लोकगीतों का सुन्दर इस्तेमाल हुआ है और भाषा शैली बहुत रोचक है .. अनिल जी ने लगभग हर पृष्ठ को छुवा है … इस समीक्षा को साझा करने के लिए शिरीष जी को धन्यवाद और अनिल जी को शुभकामनाएं